कà¥à¤¯à¤¾ हम अपनी आतà¥à¤®à¤¾ को जानते हैं?â€


Author
Manmohan Kumar AryaDate
28-Jun-2018Category
लेखLanguage
HindiTotal Views
321Total Comments
0Uploader
RajeevUpload Date
28-Jun-2018Download PDF
-0 MBTop Articles in this Category
- फलित जयोतिष पाखंड मातर हैं
- राषटरवादी महरषि दयाननद सरसवती
- राम मंदिर à¤à¥‚मि पूजन में धरà¥à¤®à¤¨à¤¿à¤°à¤ªà¥‡à¤•à¥à¤·à¤¤à¤¾ कहाठगयी? à¤à¤• लंबी सियासी और अदालती लड़ाई के बाद 5 अगसà¥à¤¤ को पà¥
- सनत गरू रविदास और आरय समाज
- बलातकार कैसे रकेंगे
Top Articles by this Author
- ईशवर
- बौदध-जैनमत, सवामी शंकराचारय और महरषि दयाननद के कारय
- अजञान मिशरित धारमिक मानयता
- यदि आरय समाज सथापित न होता तो कया होता ?
- ईशवर व ऋषियों के परतिनिधि व योगयतम उततराधिकारी महरषि दयाननद सरसवती
हम मनà¥à¤·à¥à¤¯ हैं। हमारा जनà¥à¤® माता-पिता से हà¥à¤† है। माता-पिता से मनà¥à¤·à¥à¤¯ के जनà¥à¤® की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ सृषà¥à¤Ÿà¤¿ के आरमà¥à¤ काल में मैथà¥à¤¨à¥€ सृषà¥à¤Ÿà¤¿ आरमà¥à¤ होने के साथ आरमà¥à¤ हà¥à¤ˆà¥¤ वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ में à¤à¥€ यह विदà¥à¤¯à¤®à¤¾à¤¨ है और सृषà¥à¤Ÿà¤¿ की पà¥à¤°à¤²à¤¯ होने तक यह पà¥à¤°à¤¥à¤¾ इसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° से चलती रहेगी। माता-पिता से सनà¥à¤¤à¤¾à¤¨ का जनà¥à¤® होने का सिदà¥à¤§à¤¾à¤¨à¥à¤¤ व पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ परमातà¥à¤®à¤¾ की देन है। यदि परमातà¥à¤®à¤¾ न होता और वह इस सृषà¥à¤Ÿà¤¿ को बना कर संचालित न करता तो मनà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ की उतà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ होना असमà¥à¤à¤µ था। सृषà¥à¤Ÿà¤¿ की रचना व पालन, मनà¥à¤·à¥à¤¯ आदि पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की विधि विधान पूरà¥à¤µà¤• उतà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ व जनà¥à¤® मरण तथा सà¥à¤– दà¥à¤– की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ देख कर ईशà¥à¤µà¤° की सतà¥à¤¤à¤¾ का जà¥à¤žà¤¾à¤¨ व अनà¥à¤à¤µ होता है। मनà¥à¤·à¥à¤¯ में हम दो पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° के पदारà¥à¤¥ वा पदारà¥à¤¥à¥‹à¤‚ का असà¥à¤¤à¤¿à¤¤à¥à¤µ देखते हैं। à¤à¤• जड़ पदारà¥à¤¥ है और दूसरा चेतन पदारà¥à¤¥ है। मनà¥à¤·à¥à¤¯ का शरीर जब मृतà¥à¤¯à¥ को पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होता है तो वह मृतà¥à¤¯à¥ होने पर निरà¥à¤œà¥€à¤µ व आतà¥à¤®à¤¾ विहिन होने से पूरà¥à¤£à¤¤à¤¯à¤¾ जड़ व अचेतन हो जाता है। उसे कोई कांटा चà¥à¤à¤¾à¤¯à¥‡, अंगों को काटे या फिर अगà¥à¤¨à¤¿ को समरà¥à¤ªà¤¿à¤¤ कर दे, उसे किंचित पीड़ा नहीं होती जबकि उसके जीवनकाल में à¤à¤• छोटा सा कांटा चà¥à¤à¤¨à¥‡ पर à¤à¥€ मनà¥à¤·à¥à¤¯ तड़फ उठता है। यह जो तड़फ व पीड़ा होती है यह मनà¥à¤·à¥à¤¯ शरीर में चेतन ततà¥à¤µ की विदà¥à¤¯à¤®à¤¾à¤¨à¤¤à¤¾ है। जब तक आतà¥à¤®à¤¾ शरीर में रहती है शरीर सà¥à¤– व दà¥à¤ƒà¤–, à¤à¥‚ख, पà¥à¤¯à¤¾à¤¸, रोग व शोक आदि का अनà¥à¤à¤µ करता है और जब आतà¥à¤®à¤¾ निकल जाती है तो उसे ही मृतà¥à¤¯à¥ कहते हैं। उसके बाद जो जड़ शरीर बचता है उसे किसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° की संवेदना वा सà¥à¤–, दà¥à¤ƒà¤– की अनà¥à¤à¥‚ति नहीं होती है।
हमारा व अनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का यह आतà¥à¤®à¤¾ का सà¥à¤µà¤°à¥‚प कैसा है? इसका उतà¥à¤¤à¤° है कि शरीर से सरà¥à¤µà¤¥à¤¾ à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ जीवातà¥à¤®à¤¾ à¤à¤• चेतन ततà¥à¤µ व पदारà¥à¤¥ है। मेरे शरीर में जो चेतन पदारà¥à¤¥ है वही मैं हूं। मनà¥à¤·à¥à¤¯ जब बोलता है कि मैं हूं, तो इसका अरà¥à¤¥ यह नहीं होता कि वह कह रहा है कि मैं मेरा शरीर हूं। शरीर के साथ मेरा शबà¥à¤¦ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— ही यह बता रहा है कि आतà¥à¤®à¤¾ शरीर से à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ है, शरीर सà¥à¤µà¤¯à¤‚ में वह मनà¥à¤·à¥à¤¯ नहीं है जिसके लिठमैं शबà¥à¤¦ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— करते हैं। बोलचाल में à¤à¥€ हम यह कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख आदि। यह सब पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— वैसे ही होते हैं जैसे हम कहते हैं कि मेरा पà¥à¤¤à¥à¤°, मेरा à¤à¤¾à¤ˆ, मेरे माता-पिता, मेरा घर, मेरी साईकिल व सà¥à¤•à¥‚टर, मेरे मितà¥à¤°, मेरी पà¥à¤¸à¥à¤¤à¤• आदि। जिनके साथ मेरा शबà¥à¤¦ लगता है वह मैं व मà¥à¤ से पृथक सतà¥à¤¤à¤¾ का संकेत करता है। अतः शरीर मैं नहीं हूं अपितॠयह शरीर मैं का अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤à¥ मेरी आतà¥à¤®à¤¾ का है। हमारी आतà¥à¤®à¤¾ की सतà¥à¤¤à¤¾ है। सतà¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¾à¤¨ होने से आतà¥à¤®à¤¾ सतà¥à¤¯ कहलाती है। इस आतà¥à¤®à¤¾ की उतà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ कैसे होती है? इस पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ पर विचार करते हैं तो हमें जà¥à¤žà¤¾à¤¤ होता है कि यदि हम यह कहते हैं कि आतà¥à¤®à¤¾ किसी जड़ व चेतन से उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ हà¥à¤ˆ तो फिर पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ होगा कि वह पदारà¥à¤¥, जिनसे आतà¥à¤®à¤¾ उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ हई, किससे उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ हà¥à¤? इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° विचार करते करते अनवसà¥à¤¥à¤¾ दोष उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ होगा। वेद à¤à¤µà¤‚ ऋषियों ने इस पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ का समाधान किया है। उनके अनà¥à¤¸à¤¾à¤° ईशà¥à¤µà¤°, जीव व पà¥à¤°à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ अनादि ततà¥à¤µ हैं। अनादि ततà¥à¤µ का अरà¥à¤¥ है कि उनकी कà¤à¥€ किसी अनà¥à¤¯ पदारà¥à¤¥ से उतà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ नहीं हà¥à¤ˆà¥¤ कारण या तो कारण रूप में ही रहता है या फिर वह कारà¥à¤¯ में परिणत होता है। ईशà¥à¤µà¤° व जीव यह दो à¤à¤¸à¥‡ पदारà¥à¤¥ हैं है जिनका कारण कोई नहीं और न यह किसी अनà¥à¤¯ पदारà¥à¤¥ के कारण हैं। यह सदैव अपनी अवसà¥à¤¥à¤¾ में ही रहते हैं। ईशà¥à¤µà¤° से न कोई नया पदारà¥à¤¥ बनता है और न ही आतà¥à¤®à¤¾ से कà¥à¤› बनता है। अतः आतà¥à¤®à¤¾ व जीवातà¥à¤®à¤¾ अनादि, अनà¥à¤¤à¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨, अविनाशी वा अमर पदारà¥à¤¥ हैं। गीता में बहà¥à¤¤ सà¥à¤¨à¥à¤¦à¤° रà¥à¤ª में कहा गया है ‘नैनं छिनà¥à¤¦à¤¨à¥à¤¤à¤¿ शसà¥à¤¤à¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿ नैनं दहति पावकः। न चैन कà¥à¤²à¥‡à¤¦à¤¯à¤¨à¥à¤¤à¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥‹ न शोषयति मारà¥à¤¤à¤ƒà¥¤à¥¤’ अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤à¥ आतà¥à¤®à¤¾ à¤à¤¸à¤¾ ततà¥à¤µ है जिसको शसà¥à¤¤à¥à¤° काट नहीं सकते हैं, अगà¥à¤¨à¤¿ आतà¥à¤®à¤¾ को जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायॠइसे सà¥à¤–ा नहीं सकती। परीकà¥à¤·à¤£à¥‹à¤‚ व विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ से आतà¥à¤®à¤¾ का यही सà¥à¤µà¤°à¥‚प सतà¥à¤¯ सिदà¥à¤§ होता है।
जीवातà¥à¤®à¤¾ मनà¥à¤·à¥à¤¯ शरीर में हो या अनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के शरीर में हो, यह सरà¥à¤µà¤¤à¥à¤° à¤à¤•à¤¦à¥‡à¤¶à¥€ व अलà¥à¤ªà¤œà¥à¤ž है। à¤à¤•à¤¦à¥‡à¤¶à¥€ का अरà¥à¤¥ परिमित सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ में रहने वाला सूकà¥à¤·à¥à¤® पदारà¥à¤¥ है। आतà¥à¤®à¤¾ की लमà¥à¤¬à¤¾à¤ˆ व चौडाई को न तो मिलीमीटर व उसके अंशों में वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤ किया जा सकता। इसकी लमà¥à¤¬à¤¾à¤ˆ, चौड़ाई व गोलाई को गणित की रीति से इसलिये वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤ नहीं किया जा सकता कि हम जितनी à¤à¥€ कलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ करेंगे यह उससे à¤à¥€ सूकà¥à¤·à¥à¤® है। हां, ईशà¥à¤µà¤° की सूकà¥à¤·à¥à¤®à¤¤à¤¾ की दृषà¥à¤Ÿà¤¿ से ईशà¥à¤µà¤° जीवातà¥à¤®à¤¾ से अधिक सूकà¥à¤·à¥à¤® है और आतà¥à¤®à¤¾ के à¤à¥€à¤¤à¤° वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤• रहता है। आतà¥à¤®à¤¾ ससीम है अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤à¥ परिमित है। आतà¥à¤®à¤¾ का गà¥à¤£ कहें या सà¥à¤µà¤à¤¾à¤µ यह जनà¥à¤® व मरण धरà¥à¤®à¤¾ है और करà¥à¤®à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤° उनके सà¥à¤–-दà¥à¤ƒà¤– रूपी फलों का à¤à¥‹à¤—ता है। आतà¥à¤®à¤¾ का अनेक पà¥à¤°à¤¾à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ योनियों में करà¥à¤®à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤° जनà¥à¤® होता है। वहां यह पलता व बà¥à¤¤à¤¾ है। इसमें शैशव, बाल, किशोर, यà¥à¤µà¤¾, पà¥à¤°à¥Œà¥ व वृदà¥à¤§à¤¾à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¯à¥‡à¤‚ आती हैं और फिर इसकी मृतà¥à¤¯à¥ हो जाती है। मृतà¥à¤¯à¥ के बाद इसका पà¥à¤¨à¤ƒ उसके करà¥à¤®à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° जनà¥à¤® होता है। हमारा वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ जनà¥à¤® से पूरà¥à¤µ à¤à¥€ जनà¥à¤® था, उससे पूरà¥à¤µ मृतà¥à¤¯à¥ और उससे à¤à¥€ पूरà¥à¤µà¤œà¤¨à¥à¤® था। इस कà¥à¤°à¤® व शà¥à¤°à¥ƒà¤‚खला का न तो आरमà¥à¤ है और न अनà¥à¤¤à¥¤ यह सदा से चला आ रहा है और सदैव इसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° चलता रहेगा। आतà¥à¤®à¤¾ अनादि, नितà¥à¤¯, अमर व अविनाशी पदारà¥à¤¥ है। यह न कà¤à¥€ उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ होता है और न नषà¥à¤Ÿ होता है।
हमारी आतà¥à¤®à¤¾ à¤à¤• अतà¥à¤¯à¤¨à¥à¤¤ सूकà¥à¤·à¥à¤® चेतन पदारà¥à¤¥ हैं। यही हम है और हमारा शरीर हमारा साधन है जिससे हमें अपने जीवन के उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ को पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करना है। उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ है धरà¥à¤®, अरà¥à¤¥, काम व मोकà¥à¤·à¥¤ मोकà¥à¤· अनà¥à¤¤à¤¿à¤® लकà¥à¤·à¥à¤¯ है। यह सà¤à¥€ लकà¥à¤·à¥à¤¯ मनà¥à¤·à¥à¤¯ शरीर रà¥à¤ªà¥€ साधन से पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होते हैं। इन साधनों का उलà¥à¤²à¥‡à¤– वेद और दरà¥à¤¶à¤¨ आदि गà¥à¤°à¤¨à¥à¤¥à¥‹à¤‚ सहित ऋषि दयाननà¥à¤¦ कृत गà¥à¤°à¤¨à¥à¤¥ सतà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤ªà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶ आदि में है। मत-मतानà¥à¤¤à¤°à¥‹à¤‚ के गà¥à¤°à¤¨à¥à¤¥ अविदà¥à¤¯à¤¾ से यà¥à¤•à¥à¤¤ होने के कारण न उनसे जीवन के लकà¥à¤·à¥à¤¯ को जाना जा सकता है और न उसकी पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ के साधनों को ही। अतः आतà¥à¤®à¤¾ को जानकर हमें हमें अपने उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ व लकà¥à¤·à¥à¤¯ को जानने व उसे पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने के लिठपà¥à¤°à¤¯à¤¤à¥à¤¨ करना है। लकà¥à¤·à¥à¤¯ की पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ के लिठहमें मोकà¥à¤· के साधनों को करना होगा। दरà¥à¤¶à¤¨ गà¥à¤°à¤¨à¥à¤¥ सहित इसे हम सतà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤ªà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶ के नवमॠसमà¥à¤²à¥à¤²à¤¾à¤¸ को पà¥à¤•à¤° à¤à¥€ जान सकते हैं। हमारे सà¤à¥€ ऋषि व सचà¥à¤šà¥‡ योगी इन साधनों का उपयोग करते थे। ऋषि दयाननà¥à¤¦ जी ने à¤à¥€ अपने जीवन में ईशà¥à¤µà¤°, जीवातà¥à¤®à¤¾ का जà¥à¤žà¤¾à¤¨ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ कर उसके अनà¥à¤¸à¤¾à¤° अपने करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को पूरा किया। अनà¥à¤®à¤¾à¤¨ से हम कह सकते हैं कि वह मोकà¥à¤· को पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ हो गये होंगे। मोकà¥à¤· मिलना या न मिलना ईशà¥à¤µà¤° के अधीन है और वह हमारे करà¥à¤®à¥‹à¤‚, विदà¥à¤¯à¤¾ व आचरण पर आधारित है। हम यह जानते हैं कि हमारे पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• करà¥à¤® का फल हमें मिलना है। अतः यदि हमने शà¥à¤ करà¥à¤®à¥‹à¤‚ को किया है तो निशà¥à¤šà¤¯ ही उनका परिणाम शà¥à¤ ही होगा।
जिस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° मनà¥à¤·à¥à¤¯ को मारà¥à¤œà¤¨ कर सà¥à¤µà¤šà¥à¤›à¤¤à¤¾ व पवितà¥à¤°à¤¤à¤¾ को पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करना होता है उसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° हमें यह à¤à¥€ देखना है कि हमारे चारों ओर का वातावरण पवितà¥à¤° हो। यदि नहीं है तो हमें उसके लिठपà¥à¤°à¤¾à¤£à¤ªà¤£ से पà¥à¤°à¥à¤·à¤¾à¤°à¥à¤¥ करना है। हो सकता है कि यह कारà¥à¤¯ जानलेवा à¤à¥€ हो सकता है। ऋषि के समà¥à¤®à¥à¤– à¤à¥€ हर कà¥à¤·à¤£ पà¥à¤°à¤¾à¤£ जाने के संकट रहते थे परनà¥à¤¤à¥ वह अपने करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ पालन में डटे रहते थे। विदà¥à¤µà¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ का अनà¥à¤®à¤¾à¤¨ है कि ऋषि को लगà¤à¤— 17 बार विष देकर जान से मारने के पà¥à¤°à¤¯à¤¤à¥à¤¨ किये गये परनà¥à¤¤à¥ फिर à¤à¥€ वह ईशà¥à¤µà¤° विशà¥à¤µà¤¾à¤¸ के आधार पर मनà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ करने के कारà¥à¤¯ से कà¤à¥€ चà¥à¤¯à¥à¤¤ नहीं हà¥à¤à¥¤ हमें à¤à¥€ अपने करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ का पालन करना है और दूसरों को à¤à¥€ पà¥à¤°à¥‡à¤°à¤¿à¤¤ करना है। वेद की à¤à¥€ यही आजà¥à¤žà¤¾ है। हमें समाज से अजà¥à¤žà¤¾à¤¨, अà¤à¤¾à¤µ, अनà¥à¤¯à¤¾à¤¯, हिंसा, कà¥à¤°à¥‹à¤§, लोà¤, अनाचार, दà¥à¤°à¤¾à¤šà¤¾à¤°, अà¤à¤¦à¥à¤°à¤¤à¤¾, शोषण आदि से मà¥à¤•à¥à¤¤ करना है। आतà¥à¤®à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ करना पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• मनà¥à¤·à¥à¤¯ का पहला करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ है जिसे शारीरिक उनà¥à¤¨à¤¤à¤¿ के नाम से आरà¥à¤¯à¤¸à¤®à¤¾à¤œ के नियमों में पà¥à¤°à¤¥à¤® सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ पर रखा गया है। à¤à¤¸à¤¾ करके ही समाज सà¥à¤§à¤¾à¤° हो सकता है। à¤à¤¸à¤¾ नहीं करेंगे तो कालानà¥à¤¤à¤° में यह हमें à¤à¤¸à¥€ चोट कर सकता है कि इसका विकलà¥à¤ª à¤à¥€ हमारे पास तब न होगा। अतः à¤à¤µà¤¿à¤·à¥à¤¯ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ सचेत रहते हà¥à¤ हमें वेद à¤à¤µà¤‚ सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿ पर आधारित अपने करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ सजग रहना है और समाज को सà¥à¤µà¤šà¥à¤› व पवितà¥à¤° बनाना है। ऋषि दयाननà¥à¤¦ ने शासà¥à¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ के आधार पर कहा है कि हिंसा वह होती है जो निरà¥à¤¦à¥‹à¤·à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ की जाती है। हिंसक वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ संसार में अनेक सजà¥à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ को कषà¥à¤Ÿ व दà¥à¤ƒà¤– देता है। अतः à¤à¤¸à¥‡ लोगों को हिंसा से पृथक करने के सà¤à¥€ साम, दाम, दणà¥à¤¡ व à¤à¥‡à¤¦ उपाय अपनाने उचित होते हैं। इससे समाज व सजà¥à¤œà¤¨ लोगों को सà¥à¤– पहà¥à¤‚चता है। अतः हमें अपने करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को जानना व उस पर दृण रहना है।
आतà¥à¤®à¤¾ को जाने बिना हम अपना जीवन à¤à¤²à¥€ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° से वà¥à¤¯à¤¤à¥€à¤¤ नहीं कर सकते। यदि आतà¥à¤®à¤¾ और परमातà¥à¤®à¤¾ को नहीं जानेंगे तो हमसे अधिक मातà¥à¤°à¤¾ में पाप à¤à¥€ हो सकते हैं। अतः वेद और सतà¥à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¥à¤ªà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶ आदि का निरनà¥à¤¤à¤° सà¥à¤µà¤¾à¤§à¥à¤¯à¤¾à¤¯ कर अपनी आतà¥à¤®à¤¾ व परमातà¥à¤®à¤¾ को जानें और अपने सà¤à¥€ करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯à¥‹à¤‚ का ईशà¥à¤µà¤° को साकà¥à¤·à¥€ व फलपà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¤à¤¾ मानकर पूरी निषà¥à¤ ा से पालन करें। ओ३मॠशमà¥à¥¤
-मनमोहन कà¥à¤®à¤¾à¤° आरà¥à¤¯














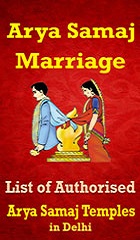
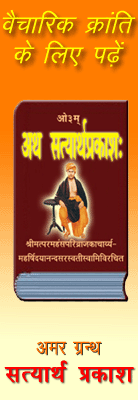



ALL COMMENTS (0)